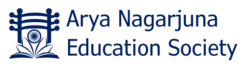नैतिकता या शील, बुद्ध और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर दोनों की शिक्षाओं में व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की नींव है। नैतिक जीवन के एक स्तंभ के रूप में, शील न केवल मानवीय रिश्तों में सामंजस्य को बढ़ावा देता है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मंच भी तैयार करता है, जो निर्वाण में परिणत होता है। यह लेख बौद्ध धर्म में शील की केंद्रीयता पर गहराई से चर्चा करता है, इसके सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण करता है, और डॉ. अंबेडकर की नैतिकता की व्याख्या को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में दर्शाता है।
बुद्ध के शिक्षाओं में शील
पाली कैनन या तिपिटक, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में शील पर चर्चाओं से भरा हुआ है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि नैतिकता वह आधार है जिस पर एकाग्रता (समाधि) और ज्ञान (पञ्ञा) का निर्माण होता है। नैतिकता, एकाग्रता और ज्ञान का यह त्रिगुणात्मक प्रशिक्षण (श्लक्षा) आर्य अष्टांगिक मार्ग (अरिय अट्ठङ्गिक मग्ग) में समाहित है।
पाँच शील: एक सार्वभौमिक नैतिक कोड
बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए नैतिकता के न्यूनतम मानक के रूप में पाँच उपदेश (पंचशील) निर्धारित किये:
- जीवित प्राणियों की हत्या से दूर रहना (पाणातिपात वेरमणी)।
- जो नहीं दिया गया है उसे लेने से बचना (अदिन्नादाना वेरमणी)।
- यौन दुराचार से दूर रहना (कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि)।
- मिथ्या भाषण से दूर रहना (मुसावादा वेरमणि)।
- मादक पेय, नशीली दवाओं और लापरवाही की ओर ले जाने वाले स्थानों से दूर रहना (सुरा-मेरयमज्ज-पमादट्ठाना वेरमणि)।
ये सिद्धांत बौद्ध धर्म के अभ्यास की नैतिक रीढ़ हैं, जो व्यक्तियों को सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने का मार्गदर्शन देते हैं तथा समाज में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
चारित्त शील और वारित्त शील
बुद्ध के शिक्षाओं में, नैतिकता को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है:
- चारित्त शील (कर्तव्यशीलता): ये सकारात्मक क्रियाएँ हैं, जिन्हें एक व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे दया दिखाना, दूसरों का सम्मान करना, और दान के कार्यों में भाग लेना। उदाहरण के लिए, सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव (मेत्ता) को विकसित करना चारित्त शील का केंद्रीय पहलू है।
- वारित्त शील (वर्जनशीलता): इसमें हानिकारक कार्यों से बचना शामिल है, जैसे हत्या, चोरी, या झूठ बोलना। पंचशील मुख्य रूप से इस श्रेणी में आते हैं, जो व्यक्तियों को ऐसे कार्यों से बचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं।
ये दोनों पहलू नैतिक जीवन की एक व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें अच्छे का सक्रिय रूप से पालन करना और बुरे से बचना शामिल है।
आध्यात्मिक प्रगति का आधार
धम्मपद में बुद्ध कहते हैं:
“सीलं रक्खंति सब्बानि, सीलं सुखं संभवं; सीलं निब्बुतिं यंति, तस्मा सीलं विसोधये।”
(धम्मपद, पद्य 183)
“शील सभी प्राणियों की रक्षा करता है; शील सुख का आधार है। शील मुक्ति की ओर ले जाता है; इसलिए, शील को शुद्ध करें।”
यह पद्य दर्शाता है कि शील दोनों सांसारिक सुख और परम मुक्ति (निर्वाण) प्राप्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाता है।
निर्वाण के मार्ग का क्रमिक विकास
“चूलहत्थिपदोम सुत्त” (मज्झिम निकाय 27) में बुद्ध निर्वाण के लिए क्रमिक मार्ग का वर्णन करते हैं, जो शील के विकास से शुरू होता है। नैतिक जीवन आत्मग्लानि से मुक्ति प्रदान करता है, जो ध्यान और अंतर्दृष्टि के विकास को सक्षम बनाता है। बुद्ध के शिक्षाएँ बार-बार यह जोर देती हैं कि शील अनुशासित और शांत चित्त के लिए नींव है, जो गहन ध्यान की अवस्थाओं और निर्वाण की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का नैतिकता पर दृष्टिकोण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एक दूरदर्शी सुधारक और सामाजिक विचारक, ने बौद्ध धर्म में नैतिकता की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचाना। उनकी व्याख्या में, शील को न केवल व्यक्तिगत अनुशासन बल्कि एक सामाजिक नैतिकता के रूप में देखा गया, जो सामाजिक समानता और मानव गरिमा को प्रोत्साहित करता है। उनकी महत्वपूर्ण कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा में, आंबेडकर ने शील को धर्म का सार बताया।
नैतिकता एक सामाजिक शक्ति के रूप में
आंबेडकर ने तर्क दिया कि नैतिकता न्याय, समानता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा:
“नैतिकता धर्म का सार है। नैतिकता के बिना, धर्म नहीं हो सकता।”
आंबेडकर के लिए, नैतिकता धार्मिक रूढ़ियों से परे है और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों में निहित है। उन्होंने बुद्ध के नैतिक शिक्षाओं को एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज बनाने के व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में देखा।
आधुनिक समाज में पंचशील की प्रासंगिकता
आंबेडकर ने विश्वास किया कि पंचशील सामाजिक समस्याओं जैसे हिंसा, असमानता, और भ्रष्टाचार का समाधान करने के लिए एक सार्वभौमिक नैतिक ढांचा प्रदान कर सकता है। इन शीलों का पालन करके, व्यक्ति और समुदाय आपसी सम्मान और सामंजस्य विकसित कर सकते हैं, जो एक अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की नींव रखते हैं।
नैतिकता और सामाजिक उत्थान
1956 में बौद्ध धर्म में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन के दौरान, आंबेडकर ने बुद्ध के शिक्षाओं की मुक्तिदायक शक्ति को उजागर किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहाँ बौद्ध सिद्धांतों में निहित नैतिकता जातिगत व्यवस्था की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बदल दे। आंबेडकर के लिए, नैतिकता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं थी, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी शक्ति थी।
शील समाज को ऊपर उठाता है
शील का अभ्यास व्यक्तिगत अखंडता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देता है। नैतिकता पर आधारित एक समाज की विशेषताएँ हैं:
- अहिंसा: दूसरों को नुकसान न पहुँचाने की प्रतिबद्धता संघर्ष को कम करती है और शांति को बढ़ावा देती है।
- विश्वासयोग्यता: असत्य और चोरी से बचने के द्वारा, व्यक्ति विश्वास बनाते हैं, जो सामाजिक एकजुटता के लिए आवश्यक है।
- सीमाओं का सम्मान: अनुचित यौनाचार से बचने से स्वस्थ संबंध बनते हैं और शोषण को रोका जा सकता है।
- सावधानी: नशे से बचने से मन की स्पष्टता सुनिश्चित होती है, जो आवेगपूर्ण और हानिकारक व्यवहार को कम करता है।
द बुद्धा एंड हिज धम्मा से अंतर्दृष्टि
द बुद्धा एंड हिज धम्मा में, डॉ. आंबेडकर ने समझाया कि कैसे नैतिकता समाज में एक बंधनकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। उन्होंने तर्क दिया:
“नैतिकता का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बुद्ध का धम्मा उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त समाज बनाने के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है।”
उन्होंने यह भी जोर दिया कि नैतिकता प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने में भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकार, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना, सुरक्षित रहें।
तिपिटक से मुख्य संदर्भ
- सामाजिक सामंजस्य में नैतिकता की भूमिका: “यत्थ सीलं तत्त्थ समाधि; यत्थ समाधि तत्त्थ पञ्ञा।” “जहाँ शील है, वहाँ ध्यान है; जहाँ ध्यान है, वहाँ प्रज्ञा।” (संयुत्त निकाय 45.1)
- सामूहिक कल्याण के लिए नैतिकता: “सीलं निब्बुतिं यंति, तस्मा सीलं विसोधये।” “शील के माध्यम से शांति प्राप्त होती है; इसलिए, शील को शुद्ध करें।” (धम्मपद, पद्य 183)
शासन में शील की भूमिका
बुद्ध के नैतिक शासन पर शिक्षाएँ, जैसे “चक्कवट्टी सीहनाद सुत्त” (दीघ निकाय 26), यह दर्शाती हैं कि शासकों को शील का पालन और प्रचार करना चाहिए। नैतिक नेतृत्व एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाता है, जो शोषण और असमानता से मुक्त होता है।
शील और निर्वाण का मार्ग
बुद्ध का मुक्ति मार्ग शील से शुरू होता है, ध्यान (समाधि) से गुजरता है, और प्रज्ञा (पञ्ञा) में समाप्त होता है। इन तीनों प्रशिक्षणों की परस्पर संबद्धता “विसुद्धिमग्ग” (पथ ऑफ प्योरीफिकेशन) में स्पष्ट है, जहाँ बुद्धघोष ने बताया कि शील आचरण को शुद्ध करता है, जिससे मन स्थिर होता है और वास्तविकता को वैसा ही देखने में सक्षम बनाता है।
क्रमिक शुद्धि
“शीलखंड” खंड, “दीघ निकाय” में, यह वर्णित है कि शील ध्यान और अंतर्दृष्टि के विकास के लिए नींव है। नैतिक नियंत्रण के बिना, मन अशांत रहता है और गहन ध्यानात्मक अवशोषण (झान) और अंतर्दृष्टि (विपस्सना) के लिए आवश्यक स्पष्टता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है।
तिपिटक से मुख्य पद्य
- ध्यान के लिए शील का समर्थन: “सीलं समाधिस्स पच्चयो होति।” “शील ध्यान की नींव है।” (अंगुत्तर निकाय 5.22)
- शील के फल: “दुक्खं पजहति, सुखं अधिगच्छति, चित्तं पसादियति।” “एक व्यक्ति दुःख को त्यागता है, सुख प्राप्त करता है, और शील के माध्यम से मन को शुद्ध करता है।” (मज्झिम निकाय 6)
निष्कर्ष
बुद्ध द्वारा परिकल्पित और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा समर्थित शील केवल नैतिक निर्देशों का एक समूह नहीं है; यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो व्यक्तियों और समाजों को ऊपर उठाती है। करुणा और प्रज्ञा में निहित, शील का अभ्यास शांति, समानता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। नैतिक सिद्धांतों का पालन करके, व्यक्ति व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सामंजस्य के लिए स्थितियाँ बनाते हैं, जो निर्वाण के अंतिम लक्ष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं।
आज की दुनिया में, जहाँ नैतिक संकट व्यापक है, बुद्ध के शिक्षाएँ और आंबेडकर का दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक हैं। शील विभाजन को दूर करने, एकता को बढ़ावा देने और मानवता की उच्चतम क्षमता को महसूस करने के लिए एक कालातीत मार्ग प्रदान करता है।